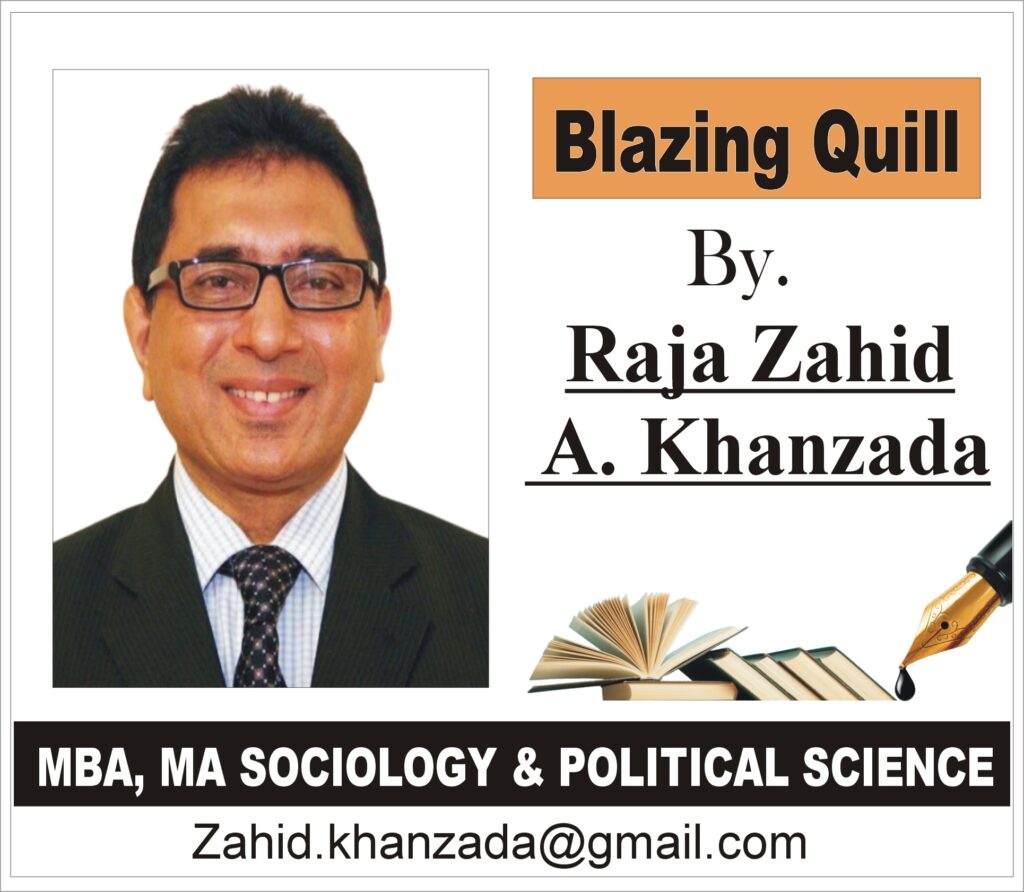दक्षिण एशिया का निर्णायक मोड़: पाकिस्तान के युद्ध ने कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया
लेखक: राजा जाहिद अख्तर ख़ानज़ादा
मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ टकराव कोई साधारण सीमा संघर्ष नहीं था—यह ताकत, तकनीक और वैश्विक नैरेटिव की लड़ाई थी। इस युद्ध की शुरुआत पहलगाम की घटना से हुई, जहाँ भारतीय नियंत्रित कश्मीर में पर्यटकों पर हुए हमले को भारत ने बिना किसी जांच के तुरंत पाकिस्तान से जोड़ते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने शुरुआत में संयम का प्रदर्शन किया, लेकिन 10 मई की सुबह जब भारत की आक्रामकता हद पार कर गई, तो पाकिस्तान ने “ऑपरेशन बुनियान मरसूस” की शुरुआत की और भारत को एक असाधारण और अप्रत्याशित अंदाज़ में जवाब दिया—और यही पल इस संघर्ष को इतिहास का मोड़ बना गया।
इस युद्ध में केवल बंदूकें नहीं बोलीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध, सेंसर फ्यूज़न और सैटेलाइट इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक हथियारों ने भी अहम भूमिका निभाई। यह लड़ाई केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की नहीं थी बल्कि यह एक मल्टी-डोमेन युद्ध था जिसमें आकाश, ज़मीन, अंतरिक्ष और डिजिटल दुनिया सभी युद्ध के मैदान बने। भारत के सबसे महंगे राफेल विमान, जिन्हें श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता था, पाकिस्तान के J-10C और PL-15 मिसाइलों के सामने बेबस हो गए। Spectra जैसे उन्नत फ्रांसीसी डिफेंस सिस्टम असफल हो गए और भारत की वायुसेना, जो हमलावर बनकर आई थी, 300 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर हो गई।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था—न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सैन्य सहयोग और तकनीकी साझेदारी के माध्यम से भी। पाकिस्तान ने जिस कुशलता से भारतीय साइबर सिस्टम्स, रेलवे नेटवर्क और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब युद्ध केवल मैदानों में नहीं, बल्कि बटन दबाकर भी लड़े जाते हैं। भारत जो खुद को राफेल और S-400 जैसे सिस्टम्स के साथ अजेय मानता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि तकनीक खरीदने और उसे समझने में ज़मीन-आसमान का फर्क होता है।
यह युद्ध केवल पाकिस्तान और भारत के बीच नहीं था—यह वैश्विक शक्तियों की परीक्षा भी थी। अमेरिका, जो शुरुआत में भारत की ओर झुकता दिखा, बाद में तटस्थ हो गया जब उसे अंदाज़ा हुआ कि पहलगाम की घटना वास्तव में भारत द्वारा किया गया एक स्व-रचित हमला था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस युद्ध से दूरी बनाने की घोषणा की, लेकिन सीआईए की ब्रीफिंग के बाद ट्रम्प प्रशासन को अपना रुख बदलना पड़ा। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत केवल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चीन से भी टकरा रहा है—और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
मोदी सरकार, जो इस युद्ध को आंतरिक राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, उल्टा उसमें फंस गई। भारतीय मीडिया ने पहले पारंपरिक शोर मचाया, लेकिन जब राफेल विमान गिरते देखे, S-400 फेल होते पाए गए, और चीन की चुप्पी महसूस की गई, तो नैरेटिव डगमगा गया। कांग्रेस और अन्य दलों ने मोदी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और भारत की राजनयिक अलगाव पूरी तरह सामने आ गई।
यह युद्ध केवल एक सीमा पर हुई झड़प नहीं थी, यह एक नई वैश्विक शक्ति-संतुलन की झलक थी। चीन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह न केवल ताइवान बल्कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपनी मर्ज़ी का माहौल बना सकता है। पाकिस्तान ने केवल रक्षा नहीं की, बल्कि अपनी रणनीति, सैन्य प्रशिक्षण और कूटनीतिक संतुलन से दुनिया को यह यकीन दिलाया कि दक्षिण एशिया का भविष्य अब पुराने सिद्धांतों से नहीं, नई तकनीक, बेहतर कूटनीति और स्मार्ट वॉरफेयर से तय होगा। यह इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसके प्रभाव न केवल क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाएंगे।
पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई न केवल आक्रामक थी बल्कि अप्रत्याशित भी—इसमें सिर्फ लक्ष्य नष्ट नहीं किए गए, बल्कि भारत की पूरी युद्ध योजना को मानसिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हिला कर रख दिया गया। जहाँ भारत ने “ऑपरेशन संदूर” के तहत पहलगाम घटना को आधार बनाकर हमले का औचित्य पेश किया, वहाँ पाकिस्तान ने “बुनियान मर्सूस” के ज़रिए यह स्पष्ट किया कि आक्रामकता का जवाब चुप्पी नहीं बल्कि अनुशासन और पूरी ताक़त के साथ दिया जाएगा।
यह कार्रवाई केवल मिसाइल फायरिंग या ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं थी। भारत के नौ सैन्य केंद्रों को निशाना बनाना, जेएफ-17 थंडर और जे-10सी के ज़रिए भारत के आधुनिक राफेल और सुखोई-30 जैसे विमानों को हवा में निष्क्रिय करना, और फिर ज़मीनी मोर्चे पर ब्रिगेड मुख्यालयों, हथियार डिपो और आपूर्ति लाइनों को तबाह करना—यह सब एक संगठित, योजनाबद्ध और उच्च पेशेवर क्षमता का प्रमाण था। भारत का एस-400 सिस्टम, जिस पर उसे बहुत गर्व था, उसका ज़मीन पर गिरना केवल तकनीकी हार नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मविश्वास का पतन था।
इन सभी घटनाओं ने भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति को भी झकझोर दिया। मोदी सरकार पर सवालों की बौछार हुई। जिन राफेल विमानों को चुनावी सफलता का हथियार बनाया गया था, वे आसमान से ज़मीन पर गिर गए। कांग्रेस ने तुरंत संसद में सवाल उठाए: “क्या हमने 250 मिलियन डॉलर प्रति विमान इसलिए खर्च किए थे कि वे कुछ सेकंडों में गिरा दिए जाएं?” भारत का मीडिया, जो शुरुआत में देशभक्ति के जोश में डूबा हुआ था, अब सरकार से सबूत मांग रहा था—कहाँ है पाकिस्तान का नुक़सान? कहाँ है तुम्हारी जीत? जवाब नहीं।
दूसरी ओर, पाकिस्तान न केवल सैन्य मोर्चे पर हावी रहा बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी उसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। तुर्की, चीन, ईरान, सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान के रुख़ का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के धैर्य और संयम की सराहना की गई। अमेरिका ने अपनी पारंपरिक पाखंड के बावजूद, युद्धविराम की मध्यस्थता की पेशकश की क्योंकि युद्ध का फैलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और भौगोलिक राजनीति के लिए ख़तरा बन चुका था।
यहाँ चीन की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चीन ने न केवल पाकिस्तान को सीधे सैन्य समर्थन दिया बल्कि इस युद्ध को एक “टेक्नोलॉजी टेस्ट” के रूप में भी इस्तेमाल किया। PL-15 मिसाइल, J-10C, सेंसर फ्यूज़न, और साइबर युद्ध के हथियारों को मैदान में आज़मा कर चीन ने पर्दे के पीछे से यह संदेश दे दिया: अगर हम ताइवान लेना चाहें, तो हमें दुनिया की अनुमति की ज़रूरत नहीं।
पाकिस्तान ने इस युद्ध में जो सफलताएँ हासिल कीं, वे केवल सैन्य प्रकृति की नहीं थीं—वे कूटनीतिक गरिमा, तकनीकी वर्चस्व और नैरेटिव की जीत थीं। जब भारत ने युद्धविराम की अपील की, तो वास्तव में वह अपनी हार स्वीकार कर रहा था, चाहे वह इसे किसी भी रूप में प्रस्तुत करे।
यह युद्ध दक्षिण एशिया के लिए एक मोड़ था। अब ताकत का संतुलन एक नए ब्लॉक की ओर झुक चुका है: पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस और तुर्की। इस ब्लॉक ने यह सिद्ध कर दिया कि अब दुनिया के फ़ैसले केवल वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में नहीं होते, बीजिंग और रावलपिंडी में भी तय होते हैं। पाकिस्तान, जिसे दुनिया कभी केवल आतंकवाद और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखती थी, अब एक आधुनिक, जागरूक और रणनीतिक रूप से स्मार्ट राष्ट्र के रूप में उभरा है।
युद्ध का अंत भले ही एक युद्धविराम पर हुआ, लेकिन इस युद्धविराम की प्रकृति औपचारिक से अधिक एक अघोषित हार की स्वीकारोक्ति थी—विशेष रूप से भारत के लिए। जब भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने शांति की पेशकश की, तो वह केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक रक्षात्मक पीछे हटने का संकेत था। पाकिस्तान ने युद्ध के मैदान में न केवल भारत की सैन्य चालों को विफल किया बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक अलगाव का भी सामना करवाया।
इस पूरे समय में पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व, विशेष रूप से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रणनीति, सहनशीलता और जवाबी शक्ति की भूमिका निर्णायक रही। पाकिस्तान ने यह साबित किया कि सैन्य प्रतिक्रिया केवल ताक़त से नहीं, बल्कि बुद्धि, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय साख से भी जीती जा सकती है।
अब सवाल यह है कि इन सब के बाद आगे क्या होगा?
भारत के लिए यह युद्ध केवल एक अस्थायी पीछे हटना नहीं बल्कि भविष्य की नीतियों में एक स्पष्ट चुनौती है। मोदी सरकार, जो स्वयं को अजेय और क्षेत्रीय चौकीदार समझती थी, अब आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर दबाव में है। चुनावी खतरे, मीडिया की आलोचना, और आर्थिक अस्थिरता ने भारतीय राज्यीय नैरेटिव को कमजोर कर दिया है। राफेल जैसे महंगे प्रोजेक्ट विफलता का प्रतीक बन चुके हैं, और S-400 की विफलता ने भारत के हथियारों पर वैश्विक भरोसे को भी हिला दिया है।
इसके विपरीत, पाकिस्तान ने इस युद्ध के माध्यम से एक नई पहचान प्राप्त की है। अब यह देश केवल एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि एक स्मार्ट वॉरफेयर शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसके पास न केवल ताकत है बल्कि सहयोगियों का समर्थन, मज़बूत नैरेटिव, और नवीनतम रक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है।
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि अब उसे वैश्विक परिदृश्य पर “समस्या” नहीं बल्कि “समाधान” के रूप में देखा जा रहा है। IMF का भरोसा बहाल हुआ, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान के रुख़ की सराहना की, और चीन, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का व्यावहारिक प्रदर्शन कर चुके हैं।
सैन्य दृष्टिकोण से, पाकिस्तानी वायुसेना ने जो प्रदर्शन किया, वह आने वाले दशकों तक क्षेत्र की युद्ध नीतियों को प्रभावित करेगा। पाकिस्तान ने न केवल दुश्मन के विमान गिराए बल्कि दुश्मन की मानसिकता पर भी चोट की—यह एक मानसिक जीत थी, जो केवल मैदान की जीत से कहीं बड़ी होती है।
यदि हम भविष्य की ओर देखें, तो अब भारत के लिए एक और युद्ध शुरू करना आसान नहीं होगा। न केवल इसके रक्षा प्रणाली पर सवाल उठ चुके हैं, बल्कि इसकी राजनीतिक नेतृत्व की निर्णय क्षमता भी अब संदेह के घेरे में आ चुकी है।
इसके विपरीत, पाकिस्तान अब एक मज़बूत, संगठित और रणनीति से भरपूर राज्य के रूप में उभरा है। इस युद्ध ने उसे एक क्षेत्रीय ब्लॉक का एक प्रमुख सदस्य बना दिया है, जो चीन, ईरान, रूस और तुर्की जैसे देशों के साथ एक नए विश्व व्यवस्था की नींव रखता है।
यह सब इस बात का संकेत है कि अब दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन केवल अर्थव्यवस्था या सैन्य उपकरणों से नहीं बल्कि नैरेटिव, तकनीक, एकता और रणनीतिक दृष्टिकोण से तय होगा—और पाकिस्तान ने इस नए युग की शुरुआत कर दी है।